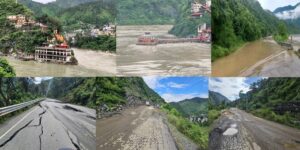जलवायु अनुकूलन की पहाड़ी कहानियां – २

जयप्रकाश पंवार ‘जेपी’
पिछले साल अजरबैजान की राजधानी बाकू में लगभग डेढ़ महीने पहले सम्पन्न हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सी.ओ.पी. 29) में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें विकसित देशों ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में, सहायता के लिए 2035 तक विकासशील देशों को प्रति वर्ष कम से कम 300 बिलियन डॉलर उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की व पेरिस समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाज़ारों के लिए तकनीकी नियमों को अंतिम रूप दिया गया। लेकिन अजब – गजब बात ये हुई की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सत्ता संभालते ही जो पहले महत्वपूर्ण निर्णय लिए वे उपरोक्त की खिलाफ निकले जैसे ट्रम्प ने कहा की वे पेरिस जलवायु समझौते से अपने को अलग करते हैं, इलेक्ट्रिक वेहिकिल की जगह पेट्रोल – डीजल को महत्व देंगे, साथ ही विश्व स्वास्थ्य संघटन से भी किनारा कर गये. अब जिन पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी कार्बन उत्सर्जन को कम करने की है वही पीछे हट जाय तो आने वाले भविष्य की तस्वीर को समझा जा सकता है. हाल की कैलिफोर्निया की भयानक आगे की घटना को वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन से जोड़ कर देख रहे हैं. इस पर भी जब अमेरिका का राष्ट्रपति संवेदनशील नहीं है तो गरीब व विकासशील देश कैसे कार्बन उत्सर्जन को कम कर पायेंगे या उसको कम करने के लिए राजस्व जुटा पायेंगे.
लौटते हैं उत्तराखंड की ओर. कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का सास्वत स्टे है. आज जिस जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, यह प्रक्रिया हजारों लाखों साल से सतत रूप से चल रही है और इस प्राकृतिक प्रक्रिया को रोकना मानव के बस में नहीं है. जब से इस धरती में जीवन की उत्पत्ति हुई है उसमे जीने के लिए एक ही उपाय होता है, जीव को बदलते प्राकृतिक माहौल के अनुसार अपने को ढालना, जो ऐसा कर पाता है और जो नहीं कर पाता उस जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है. जलवायु अनुकूलन किस तरह जीव – जंतुओं व बस्पतियों को अपने अनुसार चलने के लिए मजबूर करता है या कर रहा है इसको समझने का प्रयास करते है. उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सदियों से लोकल पहाड़ी गाय जिसे बद्री गाय भी कहा जाता है, बहुतायत में पाली जाती थी. लेकिन पिछले तीन दसकों से इस गाय का अस्तित्व समाप्त होता चला गया और अब यह लगभग संरक्षित प्रजाति की श्रेणी में आ चुकी है. टोंस घाटी के पर्वत इलाके में भैंस पालन किया जाता था, स्थानीय गांवों के लोग केदार कांठा के बुग्यालों व जंगलों में अस्थाई झोपड़ियों जिनको छानी भी कहा जाता है 6 महीने वहां रहकर भैंस पालन करते थे. चूँकि यह ईलाका गोविन्द पशु विहार संरक्षित पार्क के अंतर्गत आता है तो वन विभाग के लोगों का इनके साथ वन संरक्षण को लेकर टकराव होता रहता था. स्थानीय ग्रामीण भी इस बात से परेशान होने लगे, वे भी वनों व बुग्यालों के महत्व को समझ रहे थे. उधर गांव में लोग पहाड़ी लोकल गाय पालते, जिससे बच्चों की दूध की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. पहाड़ी गाय सुबह – शाम कुल मिलाकर औसतन एक लीटर दूध ही दे पाती थी. एक ओर भैंस पलना कठिन दूसरी ओर लोकल गाय का दूध का उत्पादन भे कम. यही पर जलवायु परिवर्तन व समय के साथ अनुकूलन होना शुरू हुआ. कोट गांव के प्रताप सिंह कहते हैं, गांव में जब से जर्सी क्रॉस ब्रीड गाय का आगमन हुआ तब से धीरे – धीरे भैंस व लोकल गाय का पालन कम होता चले गया व पिछले दो दसक में गांवों से भैंस व पहाड़ी गाय गायब हो गयी. जहाँ भैंस को गाय के मुकाबले तीन गुना चारा चाहिए था व दूध का उत्पादन भी कम था वहीँ जर्सी क्रॉस ब्रीड गाय सुबह – शाम 8 से 16 लीटर दूध का उत्पादन दे रही है. अपने उपभोग के बाद भी ग्रामीण घी बेचकर हर महीने 5 हजार से लेकर 10 हजार रुपये भी कम रहे है.

एक दूसरा रुचिकर उदाहरण देखते हैं. यमुना व टोंस घाटी में राजमा की दो प्रमुख प्रजातियाँ है लाल राजमा इसे लोग लाल कैप्सूल भी कहते हैं व चित्रा राजमा. मौसमीय बदलाव व तापमान में वृद्धि व वर्षा चक्र कैसे प्रजातियों की अदला बदली करवा देता है. यमुना घाटी के नौगांव विकासखंड का एक गांव है सरनौल, यहाँ कभी चित्रा प्रजाति की राजमा खूब पैदा होती थी. लगभग 2000 मीटर की ऊँचाई पर बसे इस गांव की ठंडी जलवायु चित्रा राजमा के लिए उपयुक्त थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इसका उत्पादन साल दर साल कम होता गया. लोगों को कुछ समझ नहीं आया. तभी किसी दुसरे गांव के लोगों ने सरनौल के किसानों को लाल राजमा को बुने की सलाह दी, पहले साल प्रयोग के तौर पर छोटे से खेत में लाल राजमा को बोया गया तो उसका उत्पादन चमत्कृत करने वाला था, फिर तो सारे गांव वालों ने लाल राजमा को उगाना शुरू किया व इसका उत्पादन चित्र के मुकाबले दुगुना हुआ व आर्थिक फायदा भी हुआ. यमुना घाटी के सरनौल गांव के उलट लगभग 130 किलोमीटर टोंस घाटी के धारकोट गंगाड गांव में लाल राजमा का बहुतायत में उत्पादन होता था, लेकिन सरनौल की तरह ही लाल राजमा का उत्पादन दर साल कम होता जा रहा था. यहाँ के ग्रामीणों को चित्रा राजमा को बोने का सुझाव दिया परिणाम चौकाने वाले थे. चित्रा राजमा का उत्पादन लाल राजमा के मुकाबले लगभग दुगुना पाया गया. वैज्ञानिकों का मानना भी रहा है कि यदि किसी प्रजाति का उत्पादन कम होने लगे तो प्रजाति में बदलाव जलवायु के साथ अनुकूलन सिखाता है.

आमतौर पर आपने सुना होगा की हिमालय की जड़ी – बूटियों में औषधीय तत्व ज्यादा होते है. ऊँची पहाड़ियों व बुग्यालों में पैदा होने वाली इन जड़ी – बूटियों का अन्दाधुन्ध दोहन होने लगा तो सरकार ने इनके दोहन को प्रतिबंधित कर दिया. लेकिन इन इलाकों के निकटस्थ गांवों में जड़ी-बूटी की खेती को प्रोत्साहित कर नया दरवाजा भी खोला. सुपिन घाटी का हिमालय के जड़ में बसे गांव रेक्चा व कासला गांवों के लोग आज जड़ी – बूटी उगाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं. कासला गांव के लक्ष्मण सिंह राणा ने जड़ी- बूटी की खेती के साथ नर्सरी भी तैयार की है, उनकी देखा देखी गांव के किसानों ने कूट की खेती करनी शुरू की, कूट की सुखी जड़ गांव से ही 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक जाती है, वहीँ इसका बीज 2500 रुपये किलो गांव में ही बिक जाता है. लक्ष्मण राणा बताते हैं की अभी उनके गोदाम में 700 किलो कूट की जड़ उपलब्ध है. इसी तरह रेक्चा के किसान केदार सिंह कुटकी की खेती करते है. कुटकी की जड़ों का बाजार भाव गांव में 90 रुपये प्रति किलो व बीज का दाम 1500 रुपये प्रति किलो है. उलेखनीय होगा कि कासला व रेक्चा जैसे 2500 मीटर से अधिक ऊँचाई पर बसे इन गांवों में, फाफरा की खेती होती थी जिसका उत्पादन कम हो रहा था व दाम भी कम मिल रहे थे, मौसमीय बदलाव ने किसानों को नए विकल्प के तौर पर जड़ी – बूटी की खेती हेतु प्रेरित किया जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिला.