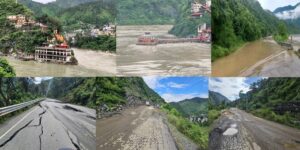भूलता सा मायका

हरीश रावत
एक और छोटी सी पहल-भूलता सा मायका, “मायका” शब्द, हृदय को छूने वाला शब्द! अब धीरे-धीरे धुंधला पड़ता जा रहा है, और प्रकृति भी थोड़ा बदल रही है, क्योंकि अब घुघुती भी नहीं बास रही है। अब किसी नव विवाहिता लड़की को अपने खेत की मुंडेर पर बैठी हुई घुघुती के घुर्र-घुर्र में, अपनी मां के स्वर नहीं सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि घुघुती भी धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही प्रजाति बन रही है, और यदि गौत्याई, घिनोड़ा के कतार में खड़ी हो गई हैं। हमारे ग्रामीण जीवन का एक मधुरतम यथार्थ है कि, चैत और बैसाख में जब प्रकृति बदलती है तो, उस बदलाव को चैतोला शब्द बड़ी आत्मियता प्रदान करता है। भाई छोटा हो या बड़ा चैतोले के दिन अपनी विवाहित बहन के लिए वस्त्र और पकवान लेकर उसके ससुराल जाना अपना सबसे प्यारा कर्तव्य समझता था और बहन भी न जाने कितने दिनों से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही होती थी।
मां या मायका, गरीब हो या अमीर हो अपने सामर्थ्य भर चैत के महीने में अपनी विवाहिता पुत्री के लिए, उसका नेग के रूप में अपना समस्त अपनत्व भेजते थे और बहुत सारे मामलों में लड़की स्वयं चैतोले के अवसर पर अपने मायके आती थी, ताकि अपने भाई-बहनों, चाचा-चाचियों व चाचा-ताऊओं और उस गांव की मिट्टी से साक्षात्कार कर सके, जिस मिट्टी में उसका जन्म हुआ। वर्ष भर में संभव हो या न हो, ससुराल वाले मायके भेजें या न भेजें, लेकिन कठोर से कठोर ससुराली भी इस मौके पर उसको मायके भेजने से इनकार नहीं कर पाते थे। चैतोले का प्रचलन कहां से प्रारंभ हुआ यह मुझे मालूम नहीं !
जब कासवा के कुंवरों ने अपनी लड़की महादेव को सौंपी तो उसके लिए भी हर वर्ष वो नेग भेजते थे, जिसको नंदा राजजात के रूप में आज भी मनाया जाता है। लेकिन चैतोला जिस महीने में मनाया जाता है, उसके बाद नंदा राजजात के प्रसंग से इसका जुड़ाव नहीं बनता है। मगर कहीं से तो यह मधुरतम प्रथा प्रारंभ हुई, एक त्योहार के रूप में प्रारंभ हुई। जब लड़की के घर भाई चैतोला लेकर जाता था तो, अपने मां के बनाए हुए पकवानों को अपने ससुरालियों व अपने ससुराल के गांव के लोगों को बाटते वक्त कितना लड़की हर्षित होती थी. इसका साक्षी बनने का मुझे भी एक-दो बार अवसर मिला है। मेरे पिताजी लोग चार भाई थे। मेरे दादा-दादी जी का मेरे पैदा होने तक स्वर्गवास हो चुका था। मगर मेरे पिताजी लोग भी अपनी दोनों बहनों को हर वर्ष चैतोला भेजते थे और अपने जीवन पर्यंत भेजते रहे, क्योंकि तब तक थोड़ा बहुत रिश्तों की समझ मुझे भी आने लग गई थी।
चार भाइयों के परिवार में चार बेटियां पैदा हुई, जिनमे से तीन स्वर्गवासी हो चुकी है, सबसे छोटी बहन गंगा जो सबसे छोटे चचा की बेटी थी अब भी हमारे पारिवारिक समारोहों के माधुर्य को बढ़ाती है, सबसे बड़ी बहन जो मेरी बड़ी मां से पैदा हुई थी उसका नाम हरी प्रिया था, उनका वो रामनगर के एक बड़े जमींदार परिवार में ब्याही थी, उसके ससुर, चचिया ससुर को राय बहादुर और राय साहब की उपाधि प्राप्त थी। मेरी दूसरे और तीसरे नंबर की बहने मेरी सबसे बड़ी चाचा की बेटी थी और छोटी बहन का नाम कमला (तमई दीदी) था, उसका बेटा आज तीसरी बार रामनगर से विधायक हैं। मेरी उस दीदी का ससुराल भी हरि दीदी के ससुराल के अड़ोस-पड़ोस में ही था। मेरी जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीदी थी वह ज्यादा दूर नहीं हमारे गांव से लगभग ढाई तीन किलोमीटर के फासले पर सुनी नामक गांव में एक अच्छे खेतिहर परिवार में ब्याही थी, इस बहन का नाम हिमवंती (हिम्मती दीदी) था। आज हमारी ये तीनों बहनें स्वर्गवासी हो चुकी हैं।
यहां तक कि मेरी एक और बहन, मामा की लड़की जो गरुड़ के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार में ब्याही थी, उसका भी स्वर्गवास हो गया है। अब केवल दो बहनें हैं, एक छोटे मामा जी की लड़की भगवती और दूसरी सबसे छोटे चाचा जी की लड़की गंगा, दोनों बहनें भी भरे पूरे परिवार की हिस्सा हैं। मैं पहले अपने स्मृति के सबसे प्यारा हिस्सा जो रामनगर में ब्याही अपनी दोनों बहनों को चैतोला देने को उद्धृत करना चाहता हूं। उन दोनों बहनों की याद मेरे मानस पटल पर उमड़-घुमड़ कर उनके द्वारा समय-समय पर मेरे प्रति दिखाया गया लाड़-प्यार लगभग 65 वर्ष बाद भी मुझे भावना के गोते खिला रहा है। मैं जीवन में पहली बार रामनगर चैतोला लेकर गया, क्योंकि जिस समय मेरी इन दोनों बहनों की शादी हुई थी उस समय रामनगर के लिए बैलगाड़ी वाली सड़क थी। मगर जब मैं चैतोला लेकर के गया रामनगर तक KMOU की बस चलती थी, बस से मुझे रामनगर भेजा गया और मेरे साथ मेरे चचेरे बड़े भाई रूद्र सिंह जी भी थे बल्कि मैं यूं कहूं कि मैं, रुद्ध सिंह जी के साथ भेजा गया था, दोनों बहनें जमींदार घरों की बहूएं थी, स्वयं बैलगाड़ी लेकर केएमयू स्टेशन आई थी।
मां ने ढेर सारे नेग के साथ पूड़ी, भरवा पूड़ी, रोट जिसको रोटाना भी कहते हैं, बड़े और भरवा लगड़, और एक विशेष चीज बनाकर के रखी थी वह था छेउआ, जो चावल का घी में तला हुआ पकवान है। उस दृश्य को याद कर मुझे आज लगभग 65 वर्ष बाद भी मेरे लिए हंसी को रोकना कठिन हो रहा है। मेरी दोनों बहनें अपने लिए भेजे गये नेग को देखने में इतनी हड़बड़ी में थी कि दोनों एक ही बैलगाड़ी में बैठ गई और दोनों ने बिना देर किए अपने-अपने हिस्से का छेउआ खा डाला। बड़ी मां को हम सभी ईजा कहते थे, वह किसी की ताई नहीं थी, मां नहीं थी, सबकी ईजा थी। जो हमारी दूसरे नंबर की बड़ी बहन थी, चैत के महीने में कभी हम उसके ससुराल जाते थे, कभी वह अपने मायके आती थी, शायद मैंने 8-9 वर्ष से अपने बड़े भाई रूद्र सिंह जी के साथ उसके ससुराल जाना शुरू किया था। वैसे परिवार में वरिष्ठता में उनका दूसरा नंबर था, हमारे बड़े भाई मोहन सिंह रावत थे वह अध्ययन के लिए बाहर रहते थे और उनके व मेरे बीच में उम्र का बहुत बड़ा अंतर था। मुझको और अन्य भाइयों को व्यवहारिकता सिखाने का काम रूद्र सिंह जी करते थे, तो कभी हम उसके गांव सूनी जाते थे, कभी वह अपने मायके आती थी। जब हम उसके गांव जाते थे, गांव की सरहद पार कर एक बड़ी सी चड़ाई लगती है, वो हमको लेने करीब पौने एक किलोमीटर की चड़ाई चढ़कर हमारे गांव की सरहद तक पहुंच जाती थी।
छोटी कद काठी की थी दीदी, बड़े इतराते हुए वह अपने मायके के उपहार को लेकर अपनी ससुराल की दहलीज पर पहुंचती थी और बड़ों के घर स्वयं जाकर ईजा के भेजे हुए त्यौहार को बाटती थी और कपड़े आदि जो भेजे जाते थे उनको अपने पास रख लेती थी। मेरी ईजा एक बात का ख्याल रखती थी कि अपनी लड़कियों के सास, जेठानी व देवरानियों के लिए भी एक-एक कपड़ा जरूर भेजती थी ताकि उनकी लड़की को उसकी जेठानी, देवरानियों और सासू मां का श्रेय प्राप्त हो सके, बहुत व्यवहारिक थी मेरी ईजा। मगर इस प्रसंग का सबसे प्यारा हिस्सा होता था जब दीदी स्वयं चैत के महीने में अपने मायके आती थी तो ईजा व चाचियां, सब उसके आने का सुबह से ही इंतजार प्रारंभ करते थे और एक-दो दिन पहले से ही दूध व दही की पराई अर्थात मलाई निकाल कर के लिए उसके लिए रख दी जाती थी और दिन देखकर के ईजा कहती थी अरे जाओ तुम्हारी दीदी आ रही होगी और हम बच्चे दौड़ लगा करके दीदी को लेने के लिए अपने गांव के आबादी के खेतों तक पहुंच जाते थे और दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई कहते हुए उसको लेकर के आते थे।
यह दृश्य अकेले हरीश रावत के जीवन का आनंदमय क्षण नहीं है, यह हर गांव, हर परिवार, हर भाई-बहन, मां-बेटी की आंतरिक भावना को चित्रित करती हुई यादें हैं जो आज विलुप्त सी हो गई हैं। आज भी कुछ पुराने परिवार हैं जो इस प्रथा का पालन करते हैं। चाहे अब उस तरीके से जैसे हरीश गया या रूद्र सिंह जी गये उस तरीके से न जाते हों, कपड़े वस्त्र आदि और कुछ नेग का रुपया जरूर बेटी-बहन को भेजते हैं। कितना इसमें प्रथा का असर है, कितना भावना का असर है, यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आशा की एक डोर बधी हुई है, मन का एक कोना कहता है कि कभी फिर आत्मीयता भरा हुआ वह चैतोला का महीना आएगा जब घुघुती भी बासेगी, जब काफल भी पकेंगे और जब नई फसल, नये पकवान अपनी बेटी का जो ससुराल वाली हो गई है उसका स्वागत करेंगे।
मेरी सरकार ने इस अमूल्य, अभूतपूर्व प्रथा को संरक्षित करने के लिए चैतोले को सरकारी तौर पर भी मानने का निर्णय लिया। यह निर्णय “म्यर गौं” अभियान का हिस्सा था। चैत के महीने के आस-पास जो लड़की अपने मायके आती थी, चाहे वह ससुराल से अपने मायके आ रही हो या प्रदेश से बाहर प्रवासित हो चुकी बेटी अपने गांव आ रही हो तो उसको गांव आने पर ग्राम प्रधान जी के माध्यम से उत्तराखंड का संस्कृति विभाग एक साड़ी और शायद ₹1000 या ₹500 नेग के रूप में दिया जाता था। यह कार्यक्रम राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा संचालित करवाया गया, मगर दुर्भाग्य से मेरी सरकार की विदाई के साथ इस शुरुआत को बंद कर दिया गया, क्यों कर दिया गया मैं नहीं जानता! लेकिन आज भी मुझे उम्मीद है कि कोई उभरता हुआ या उदीयमान होता हुआ नेता कभी इस प्रथा को संरक्षण देने के लिए आगे बढ़ेगा।
बूढ़ी दिवाली, बग्वाल भी एक ऐसा ही त्यौहार है जो राजा के विजयी होने पर लौटने के उपलक्ष में मनाया जाता था, राजशाही के कुछ हिस्सों में मनाया जाता था और इस अवसर पर भैलो खेलकर सामूहिक रूप से खुशी जाहिर की जाती है और नृत्य किया जाता है। मुझे भी कई वर्ष इस तरीके के समारोहों में भैलो खेलने का सौभाग्य मिला। जलती हुई चीड़ के राखों को जंगली लताओं से बांध कर के बड़े कलात्मक ढंग से यह भैलो खेली जाती है। संध्या के वक्त में भैलो का दृश्य बड़ा मनोहारी होता है। गांव के लोग, अड़ोस-पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर यह देखते हैं और उत्तरकाशी की रामलीला ग्राउंड में यह भैलो अभूतपु्र्व रूप से हर वर्ष खेला जाता है। देहरादून में भी जहां हमारे टिहरी के भाई-बहन आए हैं, टिहरी विस्थापित होकर वहां भी खेला जाता है। उत्तराखंड की राजनीति के एक उदीयमान बैट्समैन यदि मैं भाजपा के विराट कोहली कहूं तो यह कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी, उनकी नजर, उनकी भावना इस त्योहार से जा टकराई। यूं यह त्यौहार बूढ़ी दिवाली के रूप में राज्य भर में मनाया जाता है, कुमाऊं क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली कहते हैं और उन्होंने न केवल मनाया, बल्कि अपने गांव जाकर बड़े धूमधाम से मनाया, अपने साथ प्रभावशाली लोगों की एक टीम लेकर के गये और अब सरकार ने इसको सरकारी तौर पर मनाने का फैसला ले लिया है। यह एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि मेरा यह सुविचारित मत है कि हम दूर-दराज के गांवों से पलायन को यदि नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमको आर्थिक उपायों के साथ-साथ अपने सांस्कृतिक परिवेश और भावनात्मक परिवेश को भी, अपनी भावनात्मक ग्रामीणियत्ता को भी फिर से जागृत करना पड़ेगा।
लोक पर्व, लोक परंपरा, लोक कला, लोक साहित्य, लोक शिल्प-जोड़ती हैं। हम अपने लोक पर्वों को जितना जीवांत स्वरूप देने का प्रयास करेंगे उतनी ही हमारी ग्रामीणियत्ता लौटेगी। आज गांवों में थोड़ी संपन्नता अवश्य आयी है, मगर हम एक जुड़ाव दार ग्रामीण समाज होने के बजाय एक-दूसरे से उदासीन परिवार या पड़ोसी बनकर के रह गये हैं। इसलिये मौका पाते ही हर परिवार गांव को पीछे छोड़ दे रहा है। मैं, बार-बार इस बात को दोहराता हूं कि मैं सक्षम पलायन का विरोधी नहीं हूं। लेकिन सक्षम परिवार प्रवासित हो, मगर गांव की तरफ हमेशा पीठ फेर लें यह कठोरता मन को बहुत सालती है। हमें एक प्यार करने वाले समाज के बजाय एक कठोर समाज के रूप में हमारी पहचान बनाती है जो अच्छी बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में कई क्षेत्रों में हमसे ज्यादा कठिन जीवन है, मगर वहां के लोक पर्व, लोक कला व परंपराएं उनकी बेटी-बेटे जहां कहीं भी हैं साल में दो-तीन बार जरूर खींचकर के अपने गांव ले आती है। दक्षिण के राज्य हमसे ज्यादा विकसित भी हैं, सुसंस्कृत भी हैं, शिक्षा तकनीक आदि क्षेत्रों में बहुत आगे हैं, दुनिया भर में प्रवासित भी हैं और अच्छे मुकामों पर हैं, यहां तक कि हमारे पूर्वांचल के भाई-बंधु भी अपने लोक पर्वों के मौके पर उनके कदम स्वत: अपने गांवों की ओर चल पड़ते हैं।
सभी प्रांतों, केवल दक्षिण के नहीं हमारे पश्चिम, उत्तर के प्रांत भी, पंजाब, हिमाचल यहां भी पर्व विशेष पर अपने गांव लौटते ही लौटते हैं। हमारे राज्य में आज भी रंग संस्कृति और जौनसारी संस्कृति के लोग किसी परंपरागत लोक दिवस पर अपने गांव लौटते ही लौटते हैं। उत्तराखंड में भी पहले गर्मियों में ठंडा पानी पीने, काफल खाने लोग अपने घर आते थे, देव पूजन, जागर के लिए घर आते थे, आज देव शक्ति भी उनको एक बार भी गांव नहीं लौटा पा रही है। बल्कि मैं दिल्ली सहित चंडीगढ़ आदि कई स्थानों जैसे जालंधर, लुधियाना आदि में देखता हूँ कि लोगों ने अपने लोक देवताओं के वहीं मंदिर बना दिये हैं, वो वहीं उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। भूमियाल देवता का मंदिर जरूर बनाते हैं, लेकिन भूमि तक नहीं पहुंचते हैं। पहले हमारे गांव-घरों में पूजाई होती थी उसके लिए जो जहां होता था लाइन लगाकर के लोग आते थे, बल्कि रामनगर में मैं जब पढ़ाई करता था तो 1 महीने यह माना जाता था कि कुकल्याल रावतों की पुजाई का वक्त है, बसों में जगह नहीं मिलेगी तो रामनगर की रानीखेत रोड एक माह तक हर समय भरी-भरी रहती थी, अब कुकल्यालों की पूजा भी अपने बेटे-बेटियों को नहीं खींच पा रही है।
मैंने एक उदाहरण के तौर पर इस बात को कहा, इसलिये मैं चैतोले को एक ऐसी परंपरा मानता हूं जिसको सामाजिक और सरकारी, दोनों प्रोत्साहन यदि मिलें तो हमारे पारस्परिक बंधनों को भाई-बहन के, बेटी और मायके के बंधनों को नया जीवन दे सकता है। हमारे राज्य में ऐसे दर्जनों राज्य व्यापी और स्थानीय महत्व के त्योहार व लोक पर हैं जिन्हें संहिता बद्ध कर अपने पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। हम आगे लिए अपने नियोजन का हिस्सा न भी बनाना चाहें तो हमारी भावी पीढ़ियों को यह बताना तो आवश्यक है कि आज के यह उजड़े से गांव कभी कितने रसमय थे, जीवन का संगीत यहां अभावों में भी गुन-गुनाता था। हम यदि पलायन रोकने के लिए गंभीर हैं तो जिस सुतली से बांध कर हम अपने लोगों को गांव से जोड़ेंगे, उस सुतली को शान देने का काम हमारे ही लोक पर्व ही कर सकते हैं। ।। ॐ लोक पर्वाय नमः।।
लेखक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं