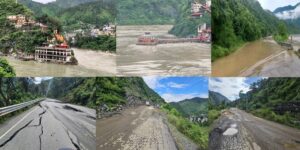शिक्षा के ज्वलंत सवाल

महावीर सिंह जगवान
प्राथमिक शिक्षा से लेकर शिक्षा के उच्च संस्थानों की उत्पादकता का एक ही पैमाना है
राष्ट्र के भावी नागरिक स्वस्थ, विवेकशील, शिक्षित, और अपने लक्ष्य का चिन्हीकरण कर अपनी योग्यता अनुशार अवसरो को प्राप्त करने की क्षमता विकसित करें। उत्तराखण्ड को शिक्षा का बड़ा केन्द्र के रूप मे विकसित करने के लिये दून विश्वविद्यालय की आधारशिला उत्तराखण्ड विधान सभा के अक्टूबर 2005 के अधिनियम के तहत रखी गई। दून विश्वविद्यालय की स्थापना का इतना बड़ा विजन था यह जे एन यू जैसीं विश्व प्रसिद्ध संस्था की तरह भविष्य मे अपना आकार लेगा। लेकिन कौशलता और राजनैतिक दूरदर्शिता के अभाव मे इतना बड़ा संस्थान विधिवत शुरूआत और के आठ नौ वर्षों के बाद भी अपनी अलग पहिचान बनाने मे अधिक सफल नही हुआ। राष्ट्र के उत्तकर्ष मे सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का ही है, भारत जैसे विकाशसील देश मे उच्चशिक्षा प्राप्त करने के बाद युवा सरकारी नौकरी मे ही आरातलबी को बरीयता देता है। शुरूआती समय मे नौकरी के लिये उच्चशिक्षा ही मानक था और योग्यतानुशार सभी को रोजगार भी सुलभ होता था।
उत्तराखण्ड मे उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिये जितना आकर्षण है इसकी प्राप्ति के बाद वर्तमान और भविष्य मे चुनौती भी विकट है।शिक्षा की पद्धतियाँ और विषयो का मकड़जाल इतना बड़ा है कि इनकी उपयोगिता ब्यवहारिक जीवन मे नगण्य है। उच्च शिक्षण संस्थानों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वह अपनी शिक्षा से राष्ट्र को सफल और शसक्त नागरिक देंगे। उत्तराखण्ड मे शिक्षा प्राप्त करने का एक ही लक्ष्य है रोजगार जबकि भारत सरकार और राज्य सरकार निरन्तर एक ही बात को दोहरा रहे हैं रोजगार के बजाय स्वरोजगार करें। सरकारी नौकरियों मे पाँच फीसदी से भी कम के अवसर हैं जबकि प्राइवेट जाॅब मे एक्सपर्ट के लिये पच्चीस फीसदी और सामान्य के लिये बीस फीसदी अवसर ही हैं, बड़ा सवाल है शिक्षा के उच्च केन्द्र पचास फीसदी अकुशल कौशल युक्त नागरिकों की भीड़ खड़ी कर रहे हैं।
यहाँ दो सवाल उभरकर आते हैं उच्च शिक्षा सरल एवं सर्व सुलभ हो या उच्च शिक्षा जटिल और कुछ लोंगो की पहुँच तक हो, यहाँ सरल और सबके लिये सुलभता के साथ उसकी उपयोगिता भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। उत्तराखण्ड मे विद्यार्थियों के पास वैकल्पिक रोजगार नहीं हैं, यहाँ पन्द्रह फीसदी अभिवाहक राजकीय सेवा मे और पन्द्रह फीसदी अभिवाहक सेना मे हैं, पचास फीसदी अभिवाहक रोजगार के लिये पलायन कर मनीआर्डर सिस्टम से परिवारों का भरण पोषण करते हैं वाकी बीस फीसदी अभिवाहक मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं इस विषम आर्थिकी के वावजूद अपने बच्चों को बालिका हो या बालक समान रूप से पूर्ण शिक्षा के लिये प्रेरित करने के साथ पूर्ण शिक्षा दिलवाते हैं। सरकारें कितना भी दावा करे सस्ती और गुणवत्ता युक्त शिक्षा की लेकिन यह कड़वी सच्चाई है शिक्षा महँगी हुई है। सरकार के जगह जगह खुलवाये विद्यालयों मे शिक्षको का भारी अकाल है और अच्छी शिक्षा की ढूँढ मे भी पलायन करना पड़ता है सामान्य आमजनमानस को अपने बच्चों की पूर्ण शिक्षा हेतु जीवन भर की तीन चौथाई कमाई खर्च करनी पड़ती है। भारत पूरे विश्व मे सबसे अधिक युवाऔं का देश है लेकिन प्रश्न इससे भी बड़ा है इन युवाऔं को तराशने वाले उच्च शिक्षण संस्थान या तो बूढे हो गये या समयानुसार परिवर्तन के अभाव मे इन युवाऔं को संकट के चौराहे पर खड़ा कर रहे हैं।
आज समय की समय से बड़ी जरूरत है शिक्षा के प्राथमिक और जूनियर ढाँचे के बाद हाई स्कूल और इण्टर की पढाई के साथ कौशल विकास की सभी इकाइयों के माॅड्यूल सम्मलित हों। इनके साथ आई टी आई और पाॅलिटेक्निक के अधिकतर विषयों का समावेश हो जाय ताकि बारहवीं तक की शिक्षा के साथ विद्यार्थी अपने पास रोजगार विषय का कौशल भी ग्रहण कर सके। स्नातक और परास्नातक के सेमिस्टरों के साथ भी कौशल विकास के ऐसे माॅड्यूल हों जो युवाऔं के पास अवसरों की पहिचान और निर्माण के लिये मजबूत साथ बने। उच्च शिक्षा को किताबी ज्ञान के साथ ब्यवहारिक ज्ञान का भी समावेश होना चाहिये।उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवा के अन्दर स्वाभिमान और हौंसलों की बुलन्दी इतनी होने चाहिये मानो देश सँवर रहा हो। राज्य और राष्ट्रों की दशा और दिशा का निर्धारण करने मे अप्रत्यक्ष रूप से सबसे बड़ी भूमिका उच्च शिक्षण संस्थाऔं की होती। राज्य सरकार और भारत सरकार को चाहिये उच्च शिक्षा केन्द्रों का नेतृत्व योग्य अनुभवी जिज्ञासु रचनाधर्मी और अनुशासित एक्सपर्टों के हाथ मे दे न कि राजनीति के आधार पर। उच्चशिक्षा की उत्पादकता पर भी गहनता से पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है। समयानुशार विषयों की उपयोगिता और चलन पर भी बहस होनी चाहिये। नये और स्थानीय जरूरतों के विषयों का भी समावेष होना चाहिये। शोध के विषयों का प्रयोगात्मक रूप से चलन बढना चाहिये। आज विश्व विद्यालयो का इतना बड़ा बजट है उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों की भूमिका और कार्यशैली मे हो रहे अमूलचूल बदलाऔं को अपनी भौगोलिक, नागरिक, अवसर, रोजगार के परिदृष्य मे परिवर्तनशील बनाना चाहिये। उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालयों के लिये उत्तराखण्ड की जैवविवधता, मानव शक्ति और अवसरों पर कार्य करने की बड़ी जरूरत है। यदि ईमानदारी से पहल होगी तो निसन्देह विश्वविद्यालयो की महत्ता बनी रहेगी। सरकारों और विश्वविद्यालयो पर भविष्य के शसक्त भविष्य की जिम्मेदारी है, समय रहते कुशल कौशल युक्त उत्पादक युवा तैयार होंगे तभी विश्व पटल पर यह कहने मे गौरव होगा हम सबसे बड़े लोकतन्त्र और सबसे अधिक युवा राष्ट्र हैं।
लेखक युवा समाजसेवी हैं